सांख्य दर्शन क्या है?
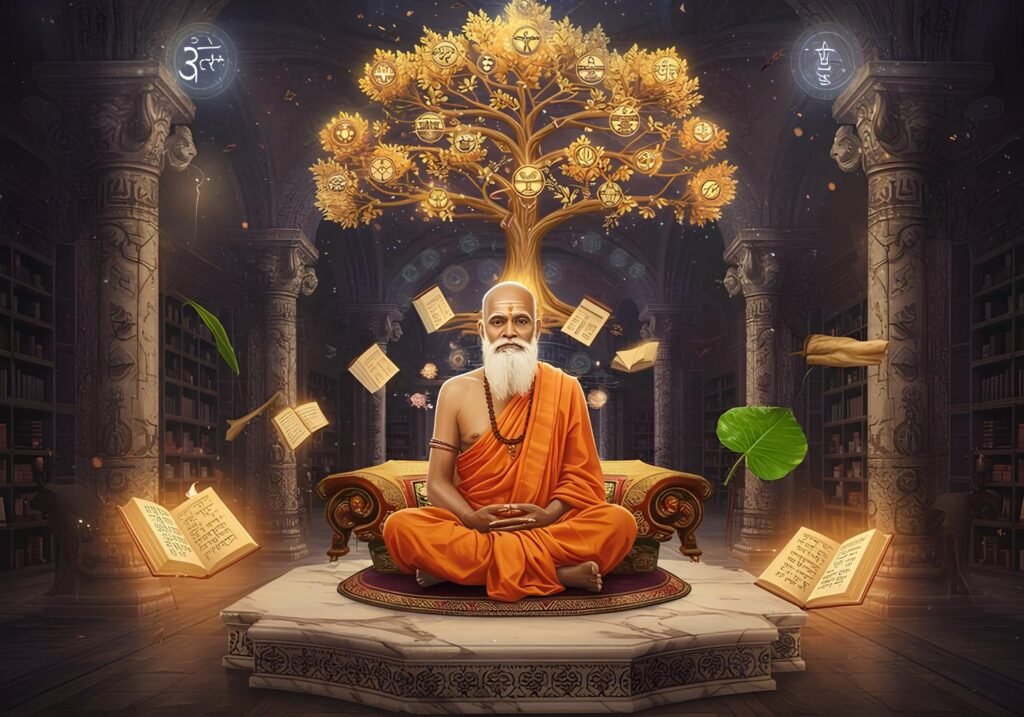
नमस्ते शिक्षणार्थियों,
इस संसार में हर एक इंसान या तो सुख पाना चाहता है अथवा अपने जीवन में आए दुखों और कष्टों का नाश करना चाहता है। हम जो भी काम करते हैं, पढाई करते हैं, नौकरी करते हैं, महनत करत हैं और पैंसे कमाते हैं – इन सब के पीछे दो ही प्रयोजन हैं सुख की प्राप्ति और दुख का परिहार। लेकिन लौकिक साधनों से प्राप्त होने वाला सुख नित्य नहीं होता। हम थोड़ी देर के लिए सुख का अनुभव करते हैं किन्तु थोड़ी देर बाद पुनः किसी अन्य कारण से दुखी हो जाते हैं अतः नित्य सुख की प्राप्ति और दुख के आत्यन्तिक परिहार के लिए ही हमारे ऋषियों ने दर्शनों का प्रणयन किया।
भारतीय ज्ञान परम्परा में ६ आस्तिक दर्शन और ३ नास्तिक दर्शनों को माना गया है। न्याय, वैशेषिक, साङ्ख्य, योग, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा (वेदान्त) – यह ३ आस्तिक दर्शन कहलाते हैं। बौद्ध, जैन और चार्वाक – ये तीन नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। यहाँ पर आस्तिक-नास्तिक का मतलब ईश्वर को मानने वाला – न मानने वाले से नहीं है क्योंकि कई ऐसे आस्तिक दर्शन भी हैं जो ईश्वर को नहीं मानते। आस्तिक और नास्तिक का यहाँ पर अर्थ है वेद को प्रमाण मानने वाला और न मानने वाला।
सांख्य दर्शन के २५ तत्त्व
दर्शनों में से साङ्ख्य दर्शन को अत्यन्त प्राचीन दर्शन माना जाता है। इसके प्रवर्तक भगवान् विष्णु के अवतार कपिल मुनि हैं। साङ्ख्य दर्शन के अनुसार मुख्य रूप से दो तत्त्व हैं – पुरुष और प्रकृति। बाद में प्रकृति के ही कार्य महत् तत्त्व, अहङ्कार आदि हैं जो कुल मिलाकर २५ तत्त्व हो जाते हैं।
मूलप्रकृतिरविकृतिर्महदाद्याः प्रकृतिविकृतयः सप्त ।
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृतिर्न विकृतिः पुरुषः ॥
वे २५ तत्त्व इस प्रकार हैं –
- प्रकृति – 1
- महत् (बुद्धि) – 1
- अहङ्कार – 1
- पञ्च तन्मात्राएं (रूप-रस-गन्ध-स्पर्श-शब्द) – 5
- पञ्च ज्ञानेन्द्रिय (नेत्र-घ्राण-रसना-श्रोत्र-त्वक्) – 5
- पञ्च कर्मेन्द्रिय {वाक्-पाद-हस्त-उपस्थ (मूत्र द्वार)-पायु (मल द्वार)} – 5
- मन – 1
- पञ्च महाभूत (पृथिवी-जल-तेज-वायु-आकाश) – 5
- पुरुष – 1
कुल तत्त्व – 1+1+1+5+5+5+1+5+1 = 25
साङ्ख्य दर्शन में ईश्वर के विषय में दो धाराएं प्रचलित हैं – सेश्वरवादी धारा तथा निरीश्वरवादी धारा। साङ्ख्य सूत्र के प्रसिद्ध भाष्यकार आचार्य विज्ञानभिक्षु ने साङ्ख्य की निरीश्वरवादी धारा को सेश्वरवाद की ओर उन्मुख किया।
तीन प्रकार के दुख
साङ्ख्य शास्त्र में तीन प्रकार के दुखों की चर्चा की गयी है – आध्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक।
दुःखत्रयाभिघाताज्जिज्ञासा तदभिघातके हेतौ ।
…………..…. श्रेयान् व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानात् ॥
- आध्यात्मिक दुख – आत्म सम्बन्धि दुख या मन से सम्बनधित दुख आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं। उदाहरण – काम, क्रोध, भय, ईर्ष्या आदि। प्रिय जन के वियोग और अप्रिय जन के संयोग से होने वाले दुख भी आध्यात्मिक दुख कहलाते हैं।
- आधिभौतिक दुख – मनुष्य द्वारा किया गया प्रहार, अन्य किसी हिंसक जीव जैसे शेर, भालू आदि द्वारा किया गया प्रहार,साँप का डसना आदि यह सब आधिभौतिक दुख के अन्तर्गत आते हैं।
- आधिदैविक दुख – भूकम्प, बाड़, बिजली गिरना, भूत – प्रेत आदि से होने वाली पीड़ा यह सब आधिदैविक दुख कहलाते हैं।
इन तीनों प्रकार के दुखों को सभी प्राणी अपने जीवन में अनुभव करते ही हैं। इन दुखों का आत्यन्तिक नाश किसी लौकिक साधन से होना संभव नहीं हैं। आप बिमार पड़ गये तो आप दवाई खाकर ठीक हो जाएंगे लेकिन दुबारा वह बिमारी अथवा अन्य कोई बिमारी आपको नहीं लगेगी इसकी कोई guarantee नहीं है। ऐसे ही कभी भी, कोई भी प्राकृतिक दुर्घटना घट सकती है और हमारा अनिष्ट हो सकता है – इन सब का निवारण लौकिक उपायों द्वारा संभव नहीं है। साङ्ख्य शास्त्र के अनुसार इन तीनों प्रकार के दुखों का आत्यन्तिक नाश संभव है। कैसे? पुरुष और प्रकृति के विवेक से। इसका तात्पर्य यह है की पुरुष यानी शुद्ध आत्मा अलग है और प्रकृति अलग है, यह विवेक – यह ज्ञान – यह साक्षात्कार जब उत्पन्न हो जाता है तब इन सभीं दुखों से जीव हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है।
प्रकृति के तीन गुण
त्रिगुणमविवेकि विषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधर्मि ।
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरीतस्तथा च पुमान् ॥
साङ्ख्य शास्त्र में तीन गुण माने गये हैं – सत्त्व, रजस् और तमस्। ये तीन गुण जिसमें सम अवस्था में रहते हैं यानी बराबर-बराबर रहते हैं वह प्रकृति कहलाती है। हर जीव-जंतु, प्राणी में, हम सब में यह तीन गुण होते ही हैं और इनका प्रभाव कम-ज़्यादा होता रहता है। कभी सत्त्व अधिक होता है, तो कभी रजो गुण और कभी तमो गुण।
सत्त्व, रजस्, तमस्
तीनों गुणों का स्वरूप
प्रीत्यप्रीतिविषादात्मकाः ……………….…।
सत्त्व, रजस्, तमस् क्रमशः सुख, दुख और मोहात्मक होते हैं। सत्त्व गुण के आधिक्य से सुख का अनुभव होता है, हम हमेशा खुश रहते हैं। रजो गुण के आधिक्य से हम दुख का अनुभव करते हैं और तमो गुण के आधिक्य से मोह यानी विषाद जिसे low feel करना कहते हैं, वैसा अनुभव करते हैं।
तीनों गुणों का कार्य
………………………. प्रकाशप्रवृत्तिनियमार्थाः ।
सत्त्व गुण का कार्य है बुद्धि का, ज्ञान का प्रकाश करना। सत्त्व गुण के आधिक्य से ही हमारा ज्ञान स्फुरित होता है। रजो गुण हमें विविध प्रकार की क्रियाओं में प्रेरित करता है और तमो गुण हमारा नियमन करता है अर्थात् न ही हम किसी ज्ञान सम्बन्धि कार्य में प्रवृत्त होते हैं और न ही खेलने – कूदने आदि क्रियाओं में, तमो गुण हमें बाँधे रखता है।
तीनों गुणों की विशेषताएं
सत्त्वं लघु प्रकाशकमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः ।
गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवच्चार्थतो वृत्तिः ॥
सत्त्व गुण हल्का होता है अर्थात् वह हमें light feel कराता है। मन का हल्का महसूस करना सत्त्व गुण का ही कार्य है। रजो गुण चञ्चल होता है, उत्तेजक होता है, कुछ न कुछ करने की चाह बनी रहती है। तमो गुण भारी होता है। पाप कर्म करने पर अनुभव होने वाला भार ही यहाँ पर विवक्षित है। ‘मन का भारी होना’ तमो गुण के आधिक्य से ही होता है। मानसिक समस्याएं जैसे किसी से बात न करना, अकेले रहना, depression आदि तमो गुण के बढने के कारण ही होती हैं। तमो गुण ज्ञान का अवरोधक भी होता है। अतः जब तमो गुण बढ जाता है तो हम कहते हैं अभी दिमाग में कुछ सूझ नहीं रहा। उसी ओर प्रातः काल सत्त्व गुण के अधिक होने से हमारा मन अध्ययन में, ज्ञान सम्बनधि कार्य में आसानी से लग जाता है।
तीनों गुणों का सार
- सत्त्वगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति स्वयं को हल्का, सुखी एवं आनन्दित अनुभव करता है।
- रजोगुण के प्रभावी होने पर व्यक्ति में चंचलता एवं गतिशीलता की अनुभूति होती है।
- तमोगुण के प्रभावी होने पर किसी भी काम को करने की इच्छा न होना, शरीर में आलस्य होना, सोने आदि में प्रवृत्त होना होता है ।
यह तीनों गुणों आपस में विरोधी हैं तभी भी इनमें अत्यधिक तालमेल रहता है। इसका उदाहरण दीप से दिया जाता है – जैसे तेल, बत्ति और अग्नि आपस में विरोधी हैं (अग्नि बत्ति को जला सकती है, बत्ति तेल सोक सकती है, तेल अग्नि को बुझा सकता है), किन्तु यह तीनों मिलकर प्रकाश रूप कार्य सम्पन्न करते हैं। ठीक उसी प्रकार सत्त्व, रजस् और तमो गुण मिलकर सृष्टि रूप कार्य सम्पन्न करते हैं।
सृष्टि का मूल कारण अव्यक्त मूलप्रकृति है जिसमें सत्त्व, रजस् और तमो गुण विद्यमान रहते हैं, इन्हीं गुणों के सहयोग से मूलप्रकृति निरन्तर क्रियाशील रहती है।
प्रकृति और पुुरुष का सम्बन्ध
पुरुषस्य दर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य ।
पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः ॥
शुद्ध आत्मा को ही साङ्ख्य दर्शन में पुरुष की संज्ञा दी गयी है और वह एक नहीं अपितु नाना है। पुरुष सत्त्व, रजस् और तमो गुण से रहित होता है अतः वह कर्ता नहीं होता, उसमें कर्तापन की प्रतीति भ्रान्तिमात्र है। पुरुष ही चेतन है बाकी सब अचेतन। पुरुष के संयोग से ही जड़ प्रकृति चेतन के समान प्रतीत होती है। पुरुष और प्रकृति का सम्बन्ध अन्धे और लंगड़े के समान है। अन्धा देख नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता अतः लंगड़ा अन्धे के कन्धे पर चढकर उसे मार्ग बताता है और अन्धा उस मार्ग पर चलता है, इससे दोनों का कार्य सिद्ध हो जाता है।
तथा च पुरुष के द्वारा प्रकृति का दर्शन और प्रकृति के द्वारा कैवल्य यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए पुरुष और प्रकृति का संयोग अन्धे और लंगड़े के समान माना गया है जिससे सृष्टि प्रक्रिया सम्पन्न होती है।
पुरुष और प्रकृति के संयोग के मुख्य दो प्रयोजन –
१. प्रकृति का दर्शन
२. पुरुष को कैवल्य की प्राप्ति
साङ्ख्य दर्शन में मोक्ष का स्वरूप है पुरुष और प्रकृति का विवेक। पुरुष अलग है और प्रकृति अलग है – इस विवेक (साक्षात्कारात्मक ज्ञान) से ही कैवल्य की प्राप्ति होती है।


